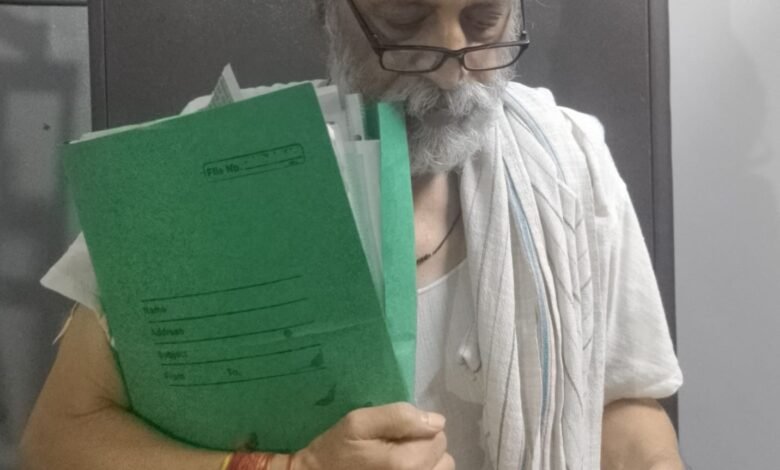
देवेंद्र कुमार बुडाकोटी
ब्रिटिश काल में, राजस्व वसूली के लिए सामंती व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था। ज़मींदार या चौधरी जैसे बड़े भू-स्वामी व्यक्तियों और गाँवों से कर वसूलते थे। इन ज़मींदारों और अधिकारियों के पास ढेरों नौकर-चाकर होते थे, जो घर और दफ्तर के कामों में सहायता करते थे। ब्रिटिश सिविल सेवक, सैन्य अधिकारी और अन्य भारतीय अफसर भी इसी तरह के सेवाओं का लाभ लेते थे। आज़ादी के बाद इन्हीं नौकरों को एक सम्मानजनक शब्द मिला — चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी — जैसे चपरासी, ड्राइवर, अर्दली आदि।
स्वतंत्र भारत ने इस परंपरा को सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में जारी रखा। निजी क्षेत्र ने भी इसी तर्ज़ पर ‘ऑफिस बॉय’ और ‘हाउसकीपिंग’ जैसे नामों से इन्हें अपनाया — अक्सर आउटसोर्स के माध्यम से। भले ही पैंट्री सिस्टम और आधुनिक सुविधाएं आ गई हों, लेकिन मानसिकता आज भी वैसी ही बनी हुई है: फाइलें उठाने, पानी-पैसे या चाय परोसने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत अब भी महसूस होती है।
यह सामंती सोच हमारे मध्यवर्गीय घरों में भी झलकती है। झाड़ू-पोंछा, बर्तन आदि के लिए अक्सर एक बाई रखी जाती है। अगर काम के लिए नौकर नहीं मिले, तो तुरंत कहा जाता है: “मुझे तो नौकर बना दिया है!” हैरानी की बात यह है कि यही लोग जब विदेश में रहते हैं, तो ये सभी काम खुद करते हैं — क्योंकि वहां मजदूरी महंगी है और प्रति घंटा भुगतान करना होता है। कुछ परिवार तो नवजात बच्चों की देखभाल के लिए मां या सास को बुला लेते हैं — एक और प्रकार की ‘अदृश्य घरेलू सहायता’।
संजय तिवारी, जो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य सरकार में सलाहकार हैं, मानते हैं कि भारत की नौकरशाही अब भी औपनिवेशिक सामंती ढांचे से ग्रस्त है। उनके अनुसार, भारत में चपरासी या ड्राइवर का होना सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि रुतबे का प्रतीक है। जबकि कनाडा में क्लर्क, सफाईकर्मी या अन्य स्टाफ काम की आवश्यकता के अनुसार होते हैं — व्यक्तिगत सेवा या अधीनता जताने के लिए नहीं। कनाडा में यूनियन, सामूहिक सौदेबाज़ी और मेरिट आधारित प्रणाली ने नौकरशाही को ज्यादा समतामूलक बनाया। भारत में ये बदलाव धीमी गति से या अधूरे रूप से हुए।
जब नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा में नए कार्यालय बने, तो कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी नाराज़गी जताई कि उन्हें अलग केबिन नहीं मिले — यह क्या दर्शाता है? सामंती मानसिकता अब भी जिंदा है।
भारत में श्रम सस्ता है, इसलिए अधिकांश शहरी मध्यवर्गीय घरों में कामवाली बाई होना सामान्य है। एक दादी ने बताया कि जब उन्होंने अपने पोते से कहा कि लॉन में गिरे पत्ते साफ करो, तो उसने जवाब दिया — “इसीलिए तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ!” सोचिए, यह कैसा दृष्टिकोण है? घर का काम अब भी “हीन” समझा जाता है।
फिर भी, जब बात सरकारी चतुर्थ श्रेणी नौकरी की होती है, तो एम.ए. और पीएच.डी धारक भी कतार में खड़े होते हैं — सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां मिलते हैं वेतन, भत्ते, रुतबा और पेंशन। निजी क्षेत्र आज तक इन बुनियादी सुविधाओं की बराबरी नहीं कर सका, इसलिए हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है।
हालांकि, अब बदलाव की आहट है। ऑफिसों में हाउसकीपिंग और कमरा सेवा जैसे कार्य आउटसोर्स हो रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम के चलते फाइलें डिजिटल हो रही हैं। अफसर अब अपने निजी वाहन से दफ्तर आ रहे हैं। क्या यह संकेत है कि तकनीकी प्रगति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के चलते सामंतवाद का अंत निकट है?
या फिर सिर्फ काम के तरीकों में बदलाव होगा, सोच अब भी वही रहेगी — यह विचारणीय प्रश्न है।




